ॐ को जानने का अर्थ है ईश्वर को जान लेना. समस्त वेद ॐ के महत्व की व्याख्या करते हैं. परमात्मा की स्तुति सृष्टि, स्थिति और प्रलय का संपादन इसी ॐ में निहीत है. सत् चित् आनंद की अनुभूति भी इसी के द्वारा संभव है. समस्त वैदिक मंत्रों का उच्चारण ॐ द्वारा ही संपन्न होता है. वेदों की ऋचाएं, श्रुतियां ॐ के उच्चारण के बिना अधूरी हैं.
जो भी ॐ का उच्चारण करता रहता है उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है. ऊँ शब्द अ, उ, म इन तीनों ध्वनियों से मिलकर बना है जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी कहा जाता है.
ॐ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का प्रदायक है। मात्र ॐ का जप कर कई साधकों ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर ली। कोशीतकी ऋषि निस्संतान थे, संतान प्राप्तिके लिए उन्होंने सूर्यका ध्यान कर ॐ का जाप किया तो उन्हे पुत्र प्राप्ति हो गई।
ॐ के उच्चारण का रहस्य
साधारण मनुष्य उस ध्वनि को सुन नहीं सकता, लेकिन जो भी ओम का उच्चारण करता रहता है उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का विकास होने लगता है। फिर भी उस ध्वनि को सुनने के लिए तो पूर्णत: मौन और ध्यान में होना जरूरी है। जो भी उस ध्वनि को सुनने लगता है वह परमात्मा से सीधा जुड़ने लगता है। परमात्मा से जुड़ने का साधारण तरीका है ॐ का उच्चारण करते रहना।
गुरु नानक जी का शब्द एक ओंकार सतनाम बहुत प्रचलित तथा शत्प्रतिशत सत्य है। एक ओंकार ही सत्य नाम है। राम, कृष्ण सब फलदायी नाम ओंकार पर निहित हैं तथा ओंकार के कारण ही इनका महत्व है। बाँकी नामों को तो हमने बनाया है परंतु ओंकार ही है जो स्वयंभू है तथा हर शब्द इससे ही बना है। हर ध्वनि में ओउ्म शब्द होता है
जो भी ॐ का उच्चारण करता रहता है उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है. ऊँ शब्द अ, उ, म इन तीनों ध्वनियों से मिलकर बना है जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी कहा जाता है.
ॐ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का प्रदायक है। मात्र ॐ का जप कर कई साधकों ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर ली। कोशीतकी ऋषि निस्संतान थे, संतान प्राप्तिके लिए उन्होंने सूर्यका ध्यान कर ॐ का जाप किया तो उन्हे पुत्र प्राप्ति हो गई।
ॐ के उच्चारण का रहस्य
साधारण मनुष्य उस ध्वनि को सुन नहीं सकता, लेकिन जो भी ओम का उच्चारण करता रहता है उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का विकास होने लगता है। फिर भी उस ध्वनि को सुनने के लिए तो पूर्णत: मौन और ध्यान में होना जरूरी है। जो भी उस ध्वनि को सुनने लगता है वह परमात्मा से सीधा जुड़ने लगता है। परमात्मा से जुड़ने का साधारण तरीका है ॐ का उच्चारण करते रहना।
त्रिदेव और त्रेलोक्य का प्रतीक
ॐ शब्द तीन ध्वनियों से बना हुआ है- अ, उ, म इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी है और यह भू: लोक, भूव: लोक और स्वर्ग लोग का प्रतीक है
ॐ शब्द तीन ध्वनियों से बना हुआ है- अ, उ, म इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी है और यह भू: लोक, भूव: लोक और स्वर्ग लोग का प्रतीक है
इसके लाभ
इससे शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलेगी। दिल की धड़कन और रक्तसंचार व्यवस्थित होगा। इससे मानसिक बीमारियाँ दूर होती हैं। काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और इसे सुनने वाला दोनों ही लाभांवित होते हैं। इसके उच्चारण में पवित्रता का ध्यान रखा जाता है।
कठोपनिषद में यह भी लिखा है कि आत्मा को अधर अरणि और ओंकार को उत्तर अरणि बनाकर मंथन रूप अभ्यास करने से दिव्य ज्ञानरूप ज्योति का आविर्भाव होता है। उसके आलोक से निगूढ़ आत्मतत्व का साक्षात्कार होता है। श्रीमद्भगवद्गीता में भी ओंकार को एकाक्षर ब्रह्म कहा है। मांडूक्योपनिषत् में भूत, भवत् या वर्तमान और भविष्य–त्रिकाल–ओंकारात्मक ही कहा गया है। यहाँ त्रिकाल से अतीत तत्व भी ओंकार ही कहा गया है। आत्मा अक्षर की दृष्टि से ओंकार है और मात्रा की दृष्टि से अ, उ और म रूप है। चतुर्थ पाद में मात्रा नहीं है एवं वह व्यवहार से अतीत तथा प्रपंचशून्य अद्वैत है। इसका अभिप्राय यह है कि ओंकारात्मक शब्द ब्रह्म और उससे अतीत परब्रह्म दोनों ही अभिन्न तत्व हैं।
इससे शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलेगी। दिल की धड़कन और रक्तसंचार व्यवस्थित होगा। इससे मानसिक बीमारियाँ दूर होती हैं। काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और इसे सुनने वाला दोनों ही लाभांवित होते हैं। इसके उच्चारण में पवित्रता का ध्यान रखा जाता है।
कठोपनिषद में यह भी लिखा है कि आत्मा को अधर अरणि और ओंकार को उत्तर अरणि बनाकर मंथन रूप अभ्यास करने से दिव्य ज्ञानरूप ज्योति का आविर्भाव होता है। उसके आलोक से निगूढ़ आत्मतत्व का साक्षात्कार होता है। श्रीमद्भगवद्गीता में भी ओंकार को एकाक्षर ब्रह्म कहा है। मांडूक्योपनिषत् में भूत, भवत् या वर्तमान और भविष्य–त्रिकाल–ओंकारात्मक ही कहा गया है। यहाँ त्रिकाल से अतीत तत्व भी ओंकार ही कहा गया है। आत्मा अक्षर की दृष्टि से ओंकार है और मात्रा की दृष्टि से अ, उ और म रूप है। चतुर्थ पाद में मात्रा नहीं है एवं वह व्यवहार से अतीत तथा प्रपंचशून्य अद्वैत है। इसका अभिप्राय यह है कि ओंकारात्मक शब्द ब्रह्म और उससे अतीत परब्रह्म दोनों ही अभिन्न तत्व हैं।
श्रीमद्मागवत् में ॐ के महत्व को कई बार रेखांकित किया गया है। श्री गीता जी के आठवें अध्याय में उल्लेख मिलता है कि जो ॐ अक्षर रूपी ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह परम गति प्राप्त करता है। ॐ अर्थात् ओउम् तीन अक्षरों से बना है, जो सर्व विदित है। अ उ म्। "अ" का अर्थ है आर्विभाव या उत्पन्न होना, "उ" का तात्पर्य है उठना, उड़ना अर्थात् विकास, "म" का मतलब है मौन हो जाना अर्थात् "ब्रह्मलीन" हो जाना। ॐ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति और पूरी सृष्टि का द्योतक है।
गुरु नानक जी का शब्द एक ओंकार सतनाम बहुत प्रचलित तथा शत्प्रतिशत सत्य है। एक ओंकार ही सत्य नाम है। राम, कृष्ण सब फलदायी नाम ओंकार पर निहित हैं तथा ओंकार के कारण ही इनका महत्व है। बाँकी नामों को तो हमने बनाया है परंतु ओंकार ही है जो स्वयंभू है तथा हर शब्द इससे ही बना है। हर ध्वनि में ओउ्म शब्द होता है
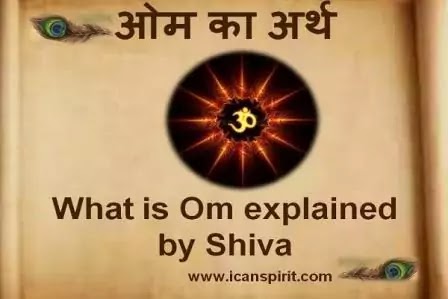





कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें